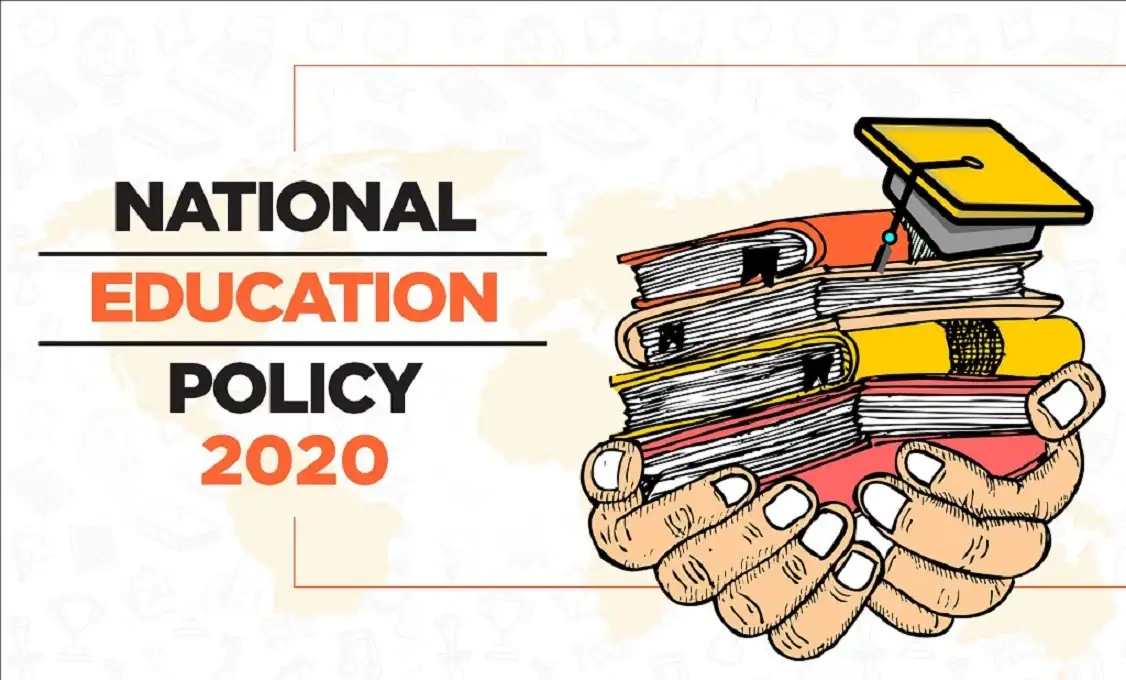CBSE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति
क्या यह नीति सच में ज़मीन पर उतरी? क्या CBSE बोर्ड और राज्य शिक्षा बोर्ड इसे लागू करने में सफल हुए?
और सबसे अहम- क्या हमारा बच्चा वाकई “रटने” से “समझने” की ओर बढ़ पाया है?
NEP 2020- शिक्षा का नया नक्शा
2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 34 साल पुरानी शिक्षा नीति (1986) की जगह ली। इसका मूल उद्देश्य था-
5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम ढाँचा,
मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता,
स्किल और प्रैक्टिकल शिक्षा पर ज़ोर,
एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली, और शोध, इनोवेशन व डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा। नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक शिक्षा में व्यापक सुधार का खाका तैयार किया गया था। CBSE और NCERT ने कहा था कि 2023 तक नए सिलेबस और मूल्यांकन प्रणाली तैयार कर ली जाएगी। परंतु, 2025 में भी न तो हर स्कूल में नया पाठ्यक्रम लागू हुआ, न हर शिक्षक को प्रशिक्षण मिला।
CBSE ने कदम तो बढ़ाए, पर मंज़िल दूर
CBSE ने 2023-24 सत्र में “Foundational Stage Curriculum Framework” जारी किया, जिसमें बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को खेल और अनुभव आधारित बनाया गया। हालांकि यह अभी केवल कुछ केन्द्रीय विद्यालयों और चुनिंदा निजी स्कूलों में प्रयोगात्मक रूप से लागू हुआ है। CBSE के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “नीति लागू करने की प्रक्रिया चरणबद्ध है। हर राज्य की तैयारी और संसाधन अलग हैं। हम नहीं चाहते कि जल्दबाज़ी में गुणवत्ता से समझौता हो।” फिर भी, परीक्षा प्रणाली, बोर्ड मूल्यांकन, और कौशल आधारित शिक्षा जैसे अहम हिस्से ज़्यादातर पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं।
NEP 2020 पर राज्यों की धीमी चाल
भारत की शिक्षा प्रणाली में 60 प्रतिशत स्कूल राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। इस कारण NEP 2020 को लागू करना केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का विषय बन गया।
केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने नए सिलेबस के कुछ हिस्सों को अपनाया है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में नीति की कई बातें अभी कागज़ों में ही सीमित हैं।
दिल्ली सरकार ने ‘Deshbhakti Curriculum’ और ‘Happiness Classes’ जैसे प्रयोग शुरू किए, जिन्हें NEP के मॉडल के अनुरूप बताया गया। परंतु इन पहलों का असर सीमित क्षेत्रों तक ही रहा। ग्रामीण स्कूलों, जहां संसाधन और प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है, वहां यह बदलाव अब तक नहीं पहुंचा।
उच्च शिक्षा में सुधार — जटिल राह
NEP 2020 के तहत UGC और AICTE को एकीकृत कर Higher Education Commission of India (HECI) बनाने की घोषणा हुई थी। यह संस्था उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता का नया ढांचा तैयार करती। परंतु अब तक यह आयोग अस्तित्व में नहीं आया है।विश्वविद्यालयों को “मल्टी-डिसिप्लिनरी” बनाने, चार-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने और Multiple Entry-Exit System शुरू करने का प्रस्ताव तो आया, पर ज़्यादातर कॉलेज आज भी पुराने तीन-वर्षीय पैटर्न पर हैं।
शिक्षकों की तैयारी सबसे बड़ी चुनौती
नीति कहती थी- “Teacher Is The Heart Of The Education System.” लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि पांच साल बीतने के बावजूद शिक्षकों के प्रशिक्षण में भारी कमी है। शिक्षा मंत्रालय की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार:
केवल 32 प्रतिशत शिक्षकों ने NEP आधारित ट्रेनिंग ली है।
सरकारी स्कूलों में 25 प्रतिशत पद रिक्त हैं।
डिजिटल प्रशिक्षण और नई मूल्यांकन प्रणाली की जानकारी सीमित है। इससे स्पष्ट है कि नीति की आत्मा- शिक्षण की गुणवत्ता, अभी अधूरी है।
डिजिटल इंडिया और शिक्षा का असंतुलन
NEP 2020 का एक बड़ा स्तंभ था- Digital Learning Revolution। COVID-19 के समय ऑनलाइन कक्षाओं ने इस दिशा में तेज़ी तो दिखाई, पर डिजिटल विभाजन ने गरीब और ग्रामीण बच्चों को पीछे छोड़ दिया। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) की स्थापना का प्रस्ताव आया, पर अब तक उसका क्रियान्वयन धीमा है। कई राज्यों में इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइस और तकनीकी संसाधनों की भारी कमी है।
मंत्रालय और प्रधानमंत्री के हालिया बयान
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा: “NEP 2020 केवल नीति नहीं, यह भारत की नई पीढ़ी को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का मिशन है। पांच वर्ष में हमने दिशा तय की है, अब गति बढ़ानी है।” शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भी कहा: “हमारी प्राथमिकता अब शिक्षकों के प्रशिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार है। NEP को अगले दो वर्षों में पूरी तरह लागू करने का रोडमैप तैयार है।” पर विशेषज्ञों का मानना है कि “रोडमैप” और “वास्तविक अमल” के बीच अब भी लंबी दूरी है।
असमानता और निजीकरण का खतरा
दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. आरती मेहता कहती हैं: “नीति बहुत दूरदर्शी है, पर ज़मीनी स्तर पर इसकी समझ बहुत सीमित है। शिक्षक और अभिभावक दोनों को इसे अपनाने में समय लगेगा।” वहीं, भारतीय शिक्षा संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रो. आलोक मिश्रा का मानना है कि: “सरकार ने नीति तो बना दी, पर लागू करने के लिए राज्यों को पर्याप्त संसाधन और स्वायत्तता नहीं दी गई।” NEP 2020 का एक और पहलू है- निजी शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन। इससे शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल और कॉलेज तो उभरे हैं, लेकिन ग्रामीण और गरीब वर्ग के लिए यह शिक्षा महंगी होती जा रही है। विशेषज्ञों का तर्क है कि शिक्षा का उद्देश्य समान अवसरदेना है, न कि वर्गों में विभाजन।
शिक्षा सुधार का अधूरा सपना
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर जब हम मौलाना आज़ाद की विरासत को याद करते हैं, तो यह सवाल उठता है- क्या आज की नीतियां शिक्षा के मूल उद्देश्य, समान अवसर, समग्र विकास और बौद्
नीति से नीयत तक: क्यों भारत में शिक्षा सुधार अटक जाता है?
हर साल 11 नवंबर को जब देश राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है, तो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की दूरदृष्टि को याद किया जाता है। उन्होंने कहा था, “कोई राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसकी शिक्षा महान हो! ” पर आज, 75 साल बाद भी, यही सबसे बड़ा सवाल है- क्या हमारी शिक्षा वास्तव में महान हुई?
नीतियां बनती रहीं, सुधारों की घोषणाएं होती रहीं, और शिक्षा के नाम पर नई योजनाओं के पोस्टर बदलते रहे। लेकिन भारत में शिक्षा सुधार हमेशा “नीति” से शुरू होकर “नीयत” पर आकर अटक जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है- काग़ज़ों पर क्रांति, ज़मीन पर धीमी चाल !
शिक्षा सुधारों का इतिहास — सपनों से समझौतों तक
आज़ादी के बाद से अब तक भारत में चार बड़ी शिक्षा नीतियां बनीं-
1. राधाकृष्णन आयोग (1948) – विश्वविद्यालय शिक्षा पर ध्यान।
2. कोठारी आयोग (1966) – “समान शिक्षा के अवसर” की वकालत।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (राजीव गांधी काल) – साक्षरता और बालिका शिक्षा को प्राथमिकता।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (मोदी सरकार) – नई पीढ़ी के अनुरूप पाठ्यक्रम और डिजिटल शिक्षा। हर नीति अपने समय की ज़रूरत थी, लेकिन हर बार एक ही गलती दोहराई गई- लक्ष्य ऊंचे, साधन कम! इरादे नेक, नीयत अधूरी!
नीति बनाम नीयत- काग़ज़ पर जो लिखा, ज़मीन पर कहां पहुंचा?
भारत में शिक्षा नीतियां हमेशा राजनीतिक दस्तावेज़ बनकर रह जाती हैं। नीति बनाना आसान है- मोटी किताबें, प्रेस कॉन्फ़्रेंस, और भाषणों में “सुधार” के शब्द ! पर असली कठिनाई है इसे जमीनी स्तर पर उतारने की नीयत और इच्छाशक्ति ! जब NEP 2020 लागू हुई, तो उम्मीद थी कि अब शिक्षा में क्रांति आएगी। पर पांच साल बाद भी शिक्षक वही, परीक्षा वही, और छात्र उसी दबाव में ! नीति कहती है, “मूल्यांकन समझ पर आधारित हो”, लेकिन स्कूल में अब भी “रटने की प्रतियोगिता” जारी है। नीयत की कमी वहां दिखती है जहां शिक्षक भर्ती राजनीति का औज़ार बन जाती है, जहां शिक्षा बजट का बड़ा हिस्सा विज्ञापनों में चला जाता है, और जहां बच्चों के सीखने की जगह “नंबरों की दौड़” को प्राथमिकता दी जाती है।
तीन दीवारें, जो शिक्षा सुधार को रोकती हैं
1. राजनीति की दीवार
भारत में शिक्षा हमेशा राजनीतिक विषय रही है- कभी आरक्षण के मुद्दे पर, कभी इतिहास की किताबों में बदलाव को लेकर, तो कभी “स्कूल ड्रेस और भाषा” पर। पर असली बहस, बच्चे कैसे सीखते हैं और क्या सी
2. अर्थ की दीवार
भारत अपने GDP का केवल 2.9 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि विकसित देशों में यह 5–6प्रतिशत तक होता है। नीतियां तभी सफल होती हैं जब उनके पीछे वित्तीय और संस्थागत ताकत हो। परंतु हमारे यहां बजट घोषणाएं तो होती हैं, पर उसका बड़ा हिस्सा वेतन और प्रशासन पर खर्च हो जाता है, न कि सुधार पर।
3. दृष्टि की दीवार
शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ़ नौकरी नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता और नागरिक चे
शिक्षक – नीति का सबसे कमजोर कड़ी
NEP 2020 में शिक्षक को ‘Nation Builder’ कहा गया, पर सच्चाई यह है कि आज़ादी के बाद से अब तक शिक्षक हमेशा “प्रशासनिक उपेक्षा” के शिकार रहे हैं। प्रशिक्षण की कमी, ओवरलोडेड काम (कभी चुनाव ड्यूटी, कभी सर्वे), और संसाधनों की कमी ने उनका मनोबल तोड़ा है। जब तक शिक्षक को नीति का “केंद्र” नहीं, “कार्यान्वयनकर्ता” माना जाएगा, तब तक शिक्षा सुधार सिर्फ़ काग़ज़ पर रहेगा।
डिजिटल युग की शिक्षा- अवसर भी, असमानता भी
NEP ने डिजिटल शिक्षा को नया युग बताया था। पर कोरोना के बाद जो सामने आया, वह “Digital Divide” की सच्चाई थी, जहां एक ओर शहरों में स्मार्ट क्लासें थीं, वहीं गावों में बच्चे मोबाइल तक से वंचित थे। नीति तो कहती है- “हर बच्चे तक तकनीक पहुंचे,” पर नीयत पूछती है- “क्या हमने सच में हर बच्चे को समान अवसर दिया?”
नीतियों की संस्कृति- सुधारों की परंपरा या दोहराव का इतिहास?
भारत में सुधारों की एक पुरानी बीमारी है, हर नई नीति पुरानी नीतियों की “कॉपी” बनकर आती है, बस भाषा बदल जाती है।
1968 में ‘कॉमन स्कूल सिस्टम’ की बात हुई- आज भी अधूरा।
1986 में ‘समान अवसर’ का वादा- आज भी असमानता बरकरार।
2020 में ‘नई शिक्षा नीति’- पांच साल बाद भी अधूरी।
नीतियां बदलती हैं, लेकिन दृष्टिकोण नहीं ! यह शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि शब्दों का पुनर्लेखन है।
समाज की भूमिका- घर से शुरू होता है सुधार
नीति और नीयत की बहस केवल सरकारों तक सीमित नहीं। समाज, माता-पिता और मीडिया- सबकी भूमिका अहम है। जब अभिभावक अपने बच्चों से केवल अंक की उम्मीद करते हैं, जब समाज शिक्षक को “सिर्फ़ नौकरी करने वाला” समझता है, और जब मीडिया शिक्षा की जगह “टॉपरों की कहानियां” दिखाता है, तब सुधार का माहौल खुद कमजोर पड़ जाता है। नीति की सफलता का असली पैमाना क्या है? सफल नीति वह नहीं जो रिपोर्टों में चमकती है, बल्कि वह है जो किसी छोटे कस्बे के स्कूल में एक बच्चे को सोचने, समझने और आत्मविश्वास से बोलने की आज़ादी देती है। जब हर बच्चा “रटने” से आगे बढ़कर “सोचने” लगेगा, तभी शिक्षा सुधार की असली मंज़िल पूरी होगी।
शिक्षा में सुधार नहीं, संस्कार चाहिए
भारत में शिक्षा सुधार की कहानी यह बताती है कि नीति से ज़्यादा ज़रूरी नीयत हो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक दृष्टि पत्र है, पर इसे हकीकत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों को एक साथ कदम बढ़ाने होंगे। जैसा कि मौलाना आज़ाद ने कहा था, “शिक्षा वह शमां है जिससे इंसानियत का हर कोना रौशन होता है।” अगर इस शमां को वाकई जलाए रखना है, तो अब नीति नहीं, अमल की बारी है।
Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!